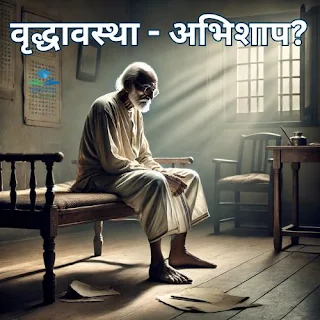|
| भारत की पहली महिला वनस्पति वैज्ञानिक |

This page offers high-quality educational resources for Hindi learners, teachers, and enthusiasts. Its goal is to support success, which is the greatest reward for our efforts. Jai Hind
यह पृष्ठ हिंदी शिक्षार्थियों, शिक्षकों और उत्साही जनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान करता है। यदि यह किसी की सफलता में योगदान दे सके, तो यही हमारे प्रयासों का पुरस्कार होगा। जय हिंद, जय हिंदी!
सोमवार, 24 मार्च 2025
❇️ गन्ने की मिठास और भारत की पहली महिला वनस्पति वैज्ञानिक
मंगलवार, 18 मार्च 2025
✨ चाँदी के लखनवी जूते: एक विलुप्त होती शाही परंपरा

जूतियाँ बनाता कारीगर
सिंड्रेला की कहानी तो आपको याद ही होगी? उस कहानी में एक विशेष जूती उसकी पहचान और भाग्य बदलने का माध्यम बनी थी। पश्चिमी दुनिया में सबसे अच्छी जूती काँच की थी, लेकिन अगर यह कथा भारतीय पृष्ठभूमि पर होती, तो वह जूती शायद चाँदी की होती - 'कलात्मक नक्काशी से सजी, लखनऊ के कुशल कारीगरों के हाथों गढ़ी हुई।' लखनऊ, जो अपनी नफासत, तहज़ीब और दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ सदियों से चाँदी के जूते बनाए जाते रहे हैं। यह परंपरा अब विलुप्ति की कगार पर है, लेकिन कुछ समर्पित शिल्पकार इसे अब भी जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं।

लखनऊ की शाही दस्तकारी: चाँदी के जूतों का इतिहास
सिंड्रेला की कहानी में जूती केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि पहचान, सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक थी। पश्चिमी लोककथाओं में यह जूती काँच की थी, लेकिन अगर यह कथा भारतीय संदर्भ में देखी जाए, तो लखनऊ का चाँदी के जूते बनाने का पारंपरिक शिल्प इससे जुड़ता हुआ प्रतीत होता है। लखनऊ, जो अपनी नजाकत, तहज़ीब और बेजोड़ कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, वहां सदियों से नगीने जड़े, हाथ से बनाए गए चाँदी के जूते एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहे हैं।
हाफिज मोहम्मद अशफाक और आफिया: एक अनमोल विरासत के संरक्षक
आज इस कला के बहुत कम कारीगर बचे हैं, लेकिन लखनऊ के हाफ़िज मोहम्मद अशफाक और उनकी बेटी आफिया इसे जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। अशफाक साहब दशकों से चाँदी की जूतियाँ बना रहे हैं, और अब उनकी बेटी आफिया भी इस हुनर को सीख रही हैं। उनका मानना है कि यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि लखनऊ की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे बचाना आवश्यक है। चाँदी के जूते बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। पहले चाँदी को पिघलाकर उसकी पतली चादर बनाई जाती है, फिर उस पर हाथ से बारीक नक्काशी की जाती है। इस प्रक्रिया में कई दिन लगते हैं, और हर जोड़ी जूती एक अनोखी कृति होती है।आधुनिकता के प्रभाव और कला का संघर्ष
फैशन के दौर में आज चाँदी के जूतों की माँग पहले जैसी नहीं रही। चमड़े, प्लास्टिक और मशीन से बने जूतों ने बाजार पर कब्जा कर लिया है। पहले जहाँ नवाबों, राजाओं और धनिकों के लिए ये जूतियाँ बनाई जाती थीं, अब इनकी माँग केवल विशेष डिजाइनरों या संग्राहकों तक सीमित रह गई है। इसके अलावा, सस्ते विकल्पों और मशीन निर्मित उत्पादों के कारण यह हस्तकला विलुप्ति के कगार पर पहुँच गई है। हालांकि, कुछ संगठनों और फैशन डिजाइनरों ने इस कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। अगर इसे वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाए, तो यह न केवल भारत की हस्तकला को पहचान दिला सकता है, बल्कि उन कारीगरों को भी नई संभावनाएँ दे सकता है जो इसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी संजोते आए हैं।
निष्कर्ष
लखनऊ की चाँदी की जूतियाँ केवल एक फैशन स्टेटस नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। यह शिल्प नवाबी दौर से जुड़ा हुआ है और लखनऊ की विशिष्टता को दर्शाता है। हफीज मोहम्मद अशफाक और आफिया जैसे कारीगर अपने हुनर और समर्पण से इसे जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाजार की प्रतिस्पर्धा और बदलते फैशन के कारण यह कला संकट में है। यदि इस अनूठी कला को उचित संरक्षण और प्रोत्साहन मिले, तो यह केवल लखनऊ ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम दे सकती है। जैसा कि सिंड्रेला की जूती ने उसकी तकदीर बदली, वैसे ही लखनऊ के चाँदी के जूते इस परंपरा को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं।
शुक्रवार, 14 मार्च 2025
गंगा-जमुनी तहज़ीब: एकता के अनमोल रंग
 |
| देवा शरीफ़ मस्जिद, बाराबंकी में होली के दीवानों ने दी एकता की मिशाल |
किन्तु यह भी सत्य है कि हाल के वर्षों में इन आपसी रिश्तों में दूरियाँ बढ़ाने की कोशिशें की गई हैं। कभी मंदिर-मस्जिद के नाम पर राजनीति होती है, तो कभी त्योहारों के दौरान संदेह और शंकाओं के बादल घिरने लगते हैं। परंतु जो लोग इस गंगा-जमुनी तहज़ीब को जीते आए हैं, उनके लिए धर्म की सीमाएँ उतनी ही बेमानी हैं जितनी नदियों के लिए उनके तटों की दीवारें। बचपन में होली पर जब मोहल्ले के हर बच्चे के चेहरे पर रंग लगा होता था, तब कोई यह नहीं पूछता था कि यह हाथ किस धर्म के हैं। नमाज से पहले रंग खेलकर मियांइन टोला के बच्चे भी अपने हिंदू दोस्तों के साथ उसी मस्ती में डूबे रहते थे।
उधर दिवाली की रात जब घर-घर दिए जलते थे, तो कई मुस्लिम परिवार अपने हिंदू मित्रों के साथ मिठाइयाँ बाँटते और उनके घरों में जाकर दीयों की रोशनी में शामिल होते।
मेरे पतिराम दादा अक्सर हमें कहानी सुनाया करते थे कि कैसे 1947 के दंगों के दौरान हमारे गाँव के हाफ़िज़ साहब ने मंदिर में छिपे हिंदू परिवारों को अपने घर ले जाकर शरण दी थी। बदले में कुछ वर्षों बाद जब उनके बेटे का निकाह था, तो पूरे गाँव ने मिलकर बारात का स्वागत किया, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम। इस भाईचारे की भावना को कोई राजनीतिक साजिश खत्म नहीं कर सकती।
भारत का इतिहास गवाह है कि यहाँ ताजमहल जितना ही महत्वपूर्ण खजुराहो के मंदिर भी हैं। कबीर की दोहों में जितना हिंदू दर्शन समाया है, उतना ही इस्लामी सूफ़ीवाद भी।
अमीर खुसरो ने हिंदवी में ऐसे गीत रचे जो आज भी दोनों समुदायों में समान रूप से गाए जाते हैं।
अगर हम बॉलीवुड की बात करें, तो मोहम्मद रफ़ी के गाए भजन और लता मंगेशकर के गाए नात दोनों ही दिल को छू लेते हैं। राही मासूम रज़ा ने 'महाभारत' की पटकथा लिखी, तो प्रेमचंद ने 'ईदगाह' के माध्यम से हिंदू-मुस्लिम एकता को जीवंत किया। यह बताता है कि हमारी साझा संस्कृति किसी एक मज़हब की जागीर नहीं, बल्कि सभी की धरोहर है।
हमारी गलियों में अब भी चाय की दुकानों पर हिंदू और मुस्लिम बुज़ुर्ग एक साथ बैठकर गप्पें लड़ाते हैं। अब भी शादी-ब्याह के मौकों पर दोनों समुदायों के लोग एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। आज भी जब कोई मुसीबत आती है, तो सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।
पर सवाल यह उठता है कि क्या हम अपनी इस साझी विरासत को बचा पाएँगे? क्या हम अपने बच्चों को यह सिखा पाएँगे कि उनका धर्म इंसानियत से ऊपर नहीं? यदि हमें अपनी संस्कृति को संजोना है, तो हमें उन ताकतों को पहचानना होगा जो हमें बाँटने की कोशिश कर रही हैं।
हमें यह स्वीकार करना होगा कि नफरत की राजनीति किसी एक धर्म को नहीं, बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुँचाती है। भारत की असली पहचान इसकी विविधता में छिपी है। यह वह देश है जहाँ कृष्ण की बांसुरी की धुन और बुल्ले शाह के कलाम एक साथ सुने जाते हैं। जहाँ गुरु नानक की वाणी और रहीम के दोहे एक ही धरती से उपजे हैं।
यह वह देश है जहाँ किसी अनाथ बच्चे को पनाह देने के लिए यह नहीं देखा जाता कि वह किस धर्म का है। अगर हमें अपने देश को सही मायनों में आगे बढ़ाना है, तो हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा। हमें फिर से उसी बचपन की मासूमियत को अपनाना होगा, जहाँ दोस्ती धर्म से बड़ी थी और मोहब्बत मज़हब से ऊपर। तभी हम इस गंगा-जमुनी तहज़ीब को हमेशा जीवित रख पाएँगे।
मंगलवार, 11 मार्च 2025
भारतीय वस्त्र विज्ञान और सूती वस्त्र
 |
| ऊन और रेशम निकालने के हिंसक विधि |
 |
| पारंपरिक भारतीय वेश में स्त्री-पुरुष |
 |
| सूती वस्त्र बनता बुनकर |
शुक्रवार, 28 फ़रवरी 2025
IBDP: Paper -1 लेखन विधाओं का सही चुनाव और मूल्यांकन मानदंड
IBDP हिंदी के प्रश्नपत्र-1 में आपको पाठ्य संकेतों (text-based prompts) के आधार पर उत्तर लिखना होता है। इसे लिखने से पूर्व सबसे बड़ी चुनौती होती है दिए गए तीनों विकल्पों में से उपयुक्त लेखन विधा का चुनाव और उसके प्रारूप व उचित संरचना का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
📌दिए गए विधाओं के विकल्पों में से हमें आमतौर पर इन्हें पहचानना आवश्यक होता है।
- ✅ उपयुक्त
- 😔सामान्यतः उपयुक्त
- ❌सामान्यतः अनुपयुक्त
- प्रश्नपत्र 1 में लेखन विधा के चयन के लिए आवश्यक नियम
- मूल्यांकन मानदंड (Assessment Criteria) और अंकदान प्रणाली
- अधिकतम अंक प्राप्त करने के सुझाव
लेखन विधा का सही चुनाव कैसे करें?
1. लेखन विधा का चयन के लिए प्रश्न की मांग को समझें
पाठ्य संकेतों को ध्यानपूर्वक पढ़े, विश्लेषण करें और समझें कि वह औपचारिक (Formal) या अनौपचारिक (Informal) लेखन की मांग कर रहा है।
| लेखन विधा | उदाहरण | प्रकार |
|---|---|---|
| लेख | समाचार पत्र, विद्यालय पत्रिका (मैगजीन) में प्रकाशन हेतु | औपचारिक |
| संपादकीय पत्र | संपादक को पत्र लिखना | औपचारिक |
| रिपोर्ट | घटनाओं या कार्यक्रम आदि की रिपोर्टिंग | औपचारिक |
| भाषण | सभा, सम्मेलन, प्रेरणादायक भाषण | औपचारिक या अनौपचारिक |
| लेख | समाचार पत्र, विद्यालय पत्रिका (मैगजीन) | औपचारिक |
| ब्लॉग | ऑनलाइन लेख, विचार-विमर्श | अनौपचारिक |
| साक्षात्कार | किसी व्यक्ति से बातचीत | औपचारिक या अनौपचारिक |
2. पाठक वर्ग (Target reader / audiance) और स्वर (Tone) का ध्यान दें।
3. सही प्रारूप का पालन और स्वर (Tone) का निर्वाह
विभिन्न लेखन विधाओं के लिए उचित प्रारूप
(A) औपचारिक लेखन विधाएँ
इन विधाओं में एक निर्धारित संरचना और औपचारिक भाषा का उपयोग किया जाता है।1. संपादकीय लेख / पत्रिका लेख
🔹 शीर्षक: संक्षिप्त और प्रभावशाली
🔹 परिचय: विषय का संक्षिप्त परिचय
🔹 मुख्य भाग: तर्क और उदाहरण सहित विषय की व्याख्या
🔹 निष्कर्ष: संक्षेप में समापन और सुझाव
2. औपचारिक पत्र
🔹 पता, तिथि, विषय, संबोधन का सही क्रम हो
🔹 संक्षिप्त और सटीक भाषा का प्रयोग करें
🔹 मुख्य मुद्दा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें
🔹 औपचारिक समापन (सादर, धन्यवाद सहित, आदि)
3. रिपोर्ट लेखन
🔹 शीर्षक: रिपोर्ट का उद्देश्य स्पष्ट करे
🔹 प्रस्तावना: घटना या विषय की पृष्ठभूमि
🔹 मुख्य भाग: तथ्य, आँकड़े, साक्षात्कार, अवलोकन आदि
🔹 निष्कर्ष: संक्षिप्त सारांश और सुझाव
(B) अनौपचारिक लेखन विधाएँ
इनमें संवादात्मक और रचनात्मक शैली का उपयोग किया जाता है।1. ब्लॉग लेखन
🔹 शीर्षक: पाठक को आकर्षित करने वाला
🔹 परिचय: विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत करें
🔹 मुख्य भाग: अनुभव, व्यक्तिगत राय, उदाहरण
🔹 निष्कर्ष: सारांश और पाठकों को विचार करने हेतु खुला छोड़ें
2. डायरी लेखन
🔹 तारीख और संबोधन (प्रिय डायरी, आदि)
🔹 स्वतंत्र और भावनात्मक भाषा
🔹 घटनाओं और विचारों की संक्षिप्त व्याख्या
🔹 समापन: आत्मविश्लेषण और भविष्य की योजनाएँ
3. साक्षात्कार लेखन
🔹 परिचय: साक्षात्कारकर्ता और विषय की जानकारी
🔹 प्रश्न-उत्तर शैली में बातचीत
🔹 संवादात्मक भाषा और सटीकता
🔹 समापन: महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश
3. प्रारूप सही न होने पर क्या समस्या होगी?
❌ उत्तर असंगठित लगेगा और परीक्षक को समझने में कठिनाई होगी।
❌ लेखन विधा की पहचान नहीं हो पाएगी, जिससे अंक कट सकते हैं।
❌ IB के मूल्यांकन मानदंडों में प्रभावशीलता और संगठन के अंक कम हो सकते हैं।
❌ औपचारिक लेखन में अनौपचारिक भाषा या अनौपचारिक लेखन में कठोर भाषा उत्तर को कमज़ोर बना सकती है।
IBDP हिंदी प्रश्नपत्र 1 का मूल्यांकन और अंकदान
IBDP पेपर 1 का मूल्यांकन चार प्रमुख मानदंडों पर आधारित होता है। (कुल 40 अंक)
| मूल्यांकन मानदंड(Criterion) | विवरण | अधिकतम अंक (40) |
|---|---|---|
| A: संप्रेषण की प्रभावशीलता (Message & Communication) | विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना | 10 |
| B: शैलीगत उपयुक्तता (Text Type & Register) | सही लेखन विधा चुनाव और स्वर का उपयोग | 10 |
| C: संगठन और संरचना (Coherence & Organization) | विचारों की तार्किक प्रस्तुति और सुव्यवस्थित संरचना | 10 |
| D: भाषा का उपयोग (Language & Accuracy) | व्याकरण, शब्दावली और भाषा की शुद्धता | 10 |
कैसे अधिकतम अंक प्राप्त करें?
✅ लेखन विधा का सही चुनाव करें।
✅ उत्तर को सुव्यवस्थित और स्पष्ट रखें।
✅ शुद्ध व्याकरण और सटीक शब्दावली का प्रयोग करें।
✅ पाठक वर्ग और उद्देश्य के अनुसार लेखन की टोन बनाए रखें।
✅ संभावित मूल्यांकन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए उत्तर लिखें।
IBDP यदि हिंदी प्रश्नपत्र-1 में सही लेखन विधा का चुनाव और मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार उत्तर लिखते हैं तो आप इस प्रश्पत्र में भी उच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं।
indicoach.blogspot.com पर अधिक पढ़ें!
बुधवार, 26 फ़रवरी 2025
सौर ऊर्जा से रोशन गुवाहाटी स्टेशन: मेरी अविस्मरणीय यात्रा
शुक्रवार, 21 फ़रवरी 2025
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भारतीय समाज पर इसका प्रभाव
भारतीय समाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव
भारत एक विकासशील देश होने के बावजूद कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से लागू कर रहा है। इसके दूरगामी प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:
1. शिक्षा और अनुसंधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता
AI ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में गहरा प्रभाव डाला है। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्म, व्यक्तिगत शिक्षण (Personalized Learning) और आभासी शिक्षक (Virtual Teachers) विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ बना रहे हैं। AI-आधारित एप्लिकेशन छात्रों को उनके सीखने के तरीके के अनुसार अनुकूलित पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। साथ ही, अनुसंधान कार्यों में भी AI का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिल रहा है।
2. स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति
स्वास्थ्य क्षेत्र में AI का उपयोग निदान, उपचार और रोगी देखभाल में हो रहा है। AI-आधारित मेडिकल चैटबॉट्स, डायग्नोस्टिक टूल्स और रोबोटिक सर्जरी ने चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन और AI-सक्षम हेल्थकेयर सिस्टम से लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है।
3. रोजगार और औद्योगिक परिवर्तन
AI ने औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हालांकि, इसने कई परंपरागत नौकरियों को खतरे में डाल दिया है, खासकर वे नौकरियाँ जो दोहराव वाले कार्यों पर आधारित थीं। हालाँकि, इसके साथ ही नए प्रकार के रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, और AI विशेषज्ञ।
4. कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का योगदान
भारत की अर्थव्यवस्था कृषि-आधारित है और AI ने इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फसल की पैदावार का पूर्वानुमान, कीट नियंत्रण, मिट्टी के विश्लेषण और सिंचाई प्रबंधन में AI तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन और सेंसर-आधारित उपकरण किसानों को उनकी फसलों की निगरानी में मदद कर रहे हैं।
5. न्यायपालिका और प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता
भारतीय न्याय व्यवस्था में भी AI का प्रयोग बढ़ रहा है। अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए AI-आधारित केस प्रेडिक्शन सिस्टम और डिजिटल केस मैनेजमेंट टूल्स का उपयोग किया जा रहा है। प्रशासनिक कार्यों में भी AI के प्रयोग से भ्रष्टाचार कम हो रहा है और सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ रही है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न चुनौतियाँ और नकारात्मक प्रभाव
- नौकरियों पर खतरा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग से कई पारंपरिक नौकरियाँ समाप्त हो सकती हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है।
- निजता और डेटा सुरक्षा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियाँ बड़े पैमाने पर डेटा एकत्र करती हैं, जिससे व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग और साइबर हमलों का खतरा बढ़ जाता है।
- नैतिक और सामाजिक चुनौतियाँ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निर्णय लेने की प्रक्रिया कभी-कभी नैतिक मानकों के अनुरूप नहीं होती, जिससे समाज में असमानता और भेदभाव की समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- तकनीकी निर्भरता: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अत्यधिक उपयोग से लोग अपने निर्णय लेने की क्षमता को कम कर सकते हैं और अत्यधिक तकनीकी निर्भरता विकसित कर सकते हैं।
निष्कर्ष
कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारतीय समाज को एक नई दिशा में ले जा रही है। यह जीवन के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। हालांकि, इसके साथ कई चुनौतियाँ भी हैं, जिनसे निपटने के लिए एक संतुलित और नैतिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। सरकार, उद्योगों और शिक्षा संस्थानों को मिलकर ऐसी रणनीतियाँ विकसित करनी चाहिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाएँ और नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करें। सही नीतियों और जागरूकता के साथ, भारत AI क्रांति का लाभ उठाकर वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है।
शनिवार, 18 जनवरी 2025
"संस्मरण: कहानी गुकेश के विश्व शतरंज चैंपियन बनने की...!🌟
 |
| शतरंज के विश्व विजेता - डी. गुकेश |
कभी-कभी जीवन में ऐसी घटनाएँ घटती हैं, जो न केवल हमें प्रेरित कर जाती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि "अनवरत मेहनत और लगन से कुछ भी असंभव नहीं है।" मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं, गुकेश दोम्मराजु (जिसे आप प्यार से 'गुकेश डी.' पुकारते हैं), एक साधारण बालक था, जिसे शतरंज की दुनिया ने असाधारण बना दिया। आज मैं अपने अनुभवों, संघर्षों और इस खेल के प्रति अपने प्रेम को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ।
शतरंज के प्रति मेरा पहला परिचय तब हुआ, जब मैं मात्र सात वर्ष का था। मेरे पिता ने एक साधारण शतरंज सेट घर लाकर दिया। उस समय मुझे इस खेल की गहराई का अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे मैंने खेलना शुरू किया, यह खेल ही मेरी दुनिया बन गया। आठ साल की उम्र में मैंने अपनी पहली प्रतियोगिता जीती। उस जीत ने मुझे यह एहसास कराया कि, 'शतरंज सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह सोचने और समझने की एक अद्भुत कला है।'
शतरंज का इतिहास भी मुझे हमेशा प्रेरित करता है। यह खेल भारत में 'चतुरंग' के रूप में शुरू हुआ, जहाँ इसे चार प्रमुख सैन्य शाखाओं का प्रतीक माना गया। यह फारस, अरब और यूरोप के रास्ते पूरी दुनिया में फैल गया। हर देश ने इसे अपनी संस्कृति के अनुसार ढाल लिया, लेकिन इसकी मूल भावना कभी नहीं बदली। शतरंज की बिसात पर हर गोटी का महत्व है, लेकिन सबसे अधिक प्रेरित करता है - 'प्यादा'। एक साधारण प्यादा भी, सही रणनीति और धैर्य के साथ, रानी बन सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है – 'मेहनत और लगन से कुछ भी बनना संभव है।' मेरे करियर में कई यादगार पल रहे हैं।
मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर खिताब जीता, वह अनुभव मेरे लिए अविस्मरणीय था। लेकिन सबसे खास दिन वह था जब मैंने ग्रैंडमास्टर का खिताब जीता। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी। यह पल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मैंने अपनी कड़ी मेहनत और गुरुजनों के मार्गदर्शन से यह सफलता हासिल की थी। मुझे आज भी याद है, जब मेरे माता-पिता की आँखों में गर्व और खुशी के आँसू थे। मुझे गर्व महसूस हो रहा है यह बताते हुए कि 12 दिसंबर 2024 को सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में, मैंने डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। 14 मैचों की इस सीरीज़ के अंतिम क्लासिकल गेम में मैंने 7.5-6.5 अंकों से जीत दर्ज की। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और उस समय मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी, जब मैंने अपने देश के नाम सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब जीता।
शतरंज ने मुझे केवल प्रतियोगिताएँ जीतने का नहीं, बल्कि जीवन को समझने का नजरिया भी दिया है। इस खेल ने मुझे सिखाया कि हर चुनौती का सामना धैर्य और योजना के साथ करना चाहिए। मैंने सीखा कि असफलताएँ केवल सीढ़ियाँ हैं, जो हमें सफलता तक ले जाती हैं। मेरी हर हार ने मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।
आज, मैं आप सभी से यही कहता हूँ कि शतरंज सिर्फ एक खेल नहीं है। यह जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन, रणनीति और सोचने की क्षमता विकसित करता है। यदि आप शतरंज खेलते हैं, तो यह न केवल आपके दिमाग को तेज़ करेगा, बल्कि आपको धैर्य और संघर्ष का महत्व भी सिखाएगा। तो, प्रिय छात्रों, जीवन की बिसात पर अपनी चालें सोच-समझकर चलिए। मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास से आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
निम्नलिखित शब्दों के अर्थ जानने के लिए उन पर कर्सर ले जाएँ:
घटना Event , प्रेरित Inspired , अनवरत Continuous , मेहनत Hard work , लगन Dedication , साधारण Ordinary , असाधारण Extraordinary , अनुभव Experience , संघर्ष Struggle , प्रतियोगिता Competition , गहराई Depth , अद्भुत Wonderful , इतिहास History , चतुरंग Chaturanga (Ancient Indian Game) , सैन्य Army , शाखा Branch , प्रतीक Symbol , प्यादा Pawn (Chess Piece) , रानी Queen (Chess Piece) , रणनीति Strategy , धैर्य Patience , गुरुजन Teachers/Guides , खिताब Title , अविस्मरणीय Unforgettable , ग्रैंडमास्टर Grandmaster , गर्व Pride , चैंपियनशिप Championship , फाइनल Final , क्लासिकल Classical , अंक Points , उपलब्धि Achievement , सीढ़ियाँ Steps , धैर्य Patience , अनुशासन Discipline , दिशा Direction , चालें Moves .।
बुधवार, 15 जनवरी 2025
🌟संस्कृति के शुभ प्रतीक: एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर 🌟
 |
| हमारी संस्कृति के शुभ प्रतीक |
ॐ (ओम) भारतीय धर्मों, विशेषकर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अत्यधिक पूजनीय है। यह ध्वनि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अस्तित्व का प्रतीक है। इसे ध्यान और साधना का मुख्य मंत्र माना जाता है। ओम का उच्चारण मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्मिक शुद्धता प्रदान करता है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को प्रकट करता है। दीपक भारतीय संस्कृति में प्रकाश, ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। दीपक का प्रज्वलन अंधकार को दूर करने और जीवन में ज्ञान के प्रकाश को लाने का संदेश देता है। दीपावली जैसे त्योहारों में दीपकों का विशेष महत्त्व होता है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाते हैं।
कमल का फूल पवित्रता, आध्यात्मिकता और सौंदर्य का प्रतीक है। यह भारतीय धर्मग्रंथों और कला में व्यापक रूप से प्रचलित है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कमल पर विराजमान दिखाया जाता है, जो इसे दिव्यता और समृद्धि का प्रतीक बनाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों के बीच भी पवित्र और अडिग रहना चाहिए। गाय भारतीय संस्कृति में माता के रूप में पूजनीय है। इसे जीवनदायिनी और करुणा का प्रतीक माना जाता है। गाय का दूध, घी, और अन्य उत्पाद न केवल पोषण प्रदान करते हैं, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी इनका उपयोग होता है। गाय को भारतीय संस्कृति में शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है।
पीपल का वृक्ष भारतीय संस्कृति में दिव्यता और अनंतता का प्रतीक है। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान माना जाता है। पीपल के नीचे ध्यान करने से मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह वृक्ष पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। चक्र भारतीय तिरंगे में मध्य में स्थित है और इसे धर्मचक्र कहा जाता है। यह कर्म, धर्म और समय के सतत प्रवाह का प्रतीक है। चक्र हमें जीवन में गतिशील और कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देता है। यह भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है।
हल्दी और कुंकुम शुभता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक हैं। धार्मिक अनुष्ठानों, विवाह और अन्य शुभ कार्यों में इनका उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। हल्दी को औषधीय गुणों के कारण भी महत्त्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी भारतीय संस्कृति में धार्मिक और औषधीय दृष्टि से अत्यधिक पूजनीय है। इसे माता तुलसी के रूप में पूजा जाता है और घर में इसकी उपस्थिति शुभ मानी जाती है। तुलसी का पौधा न केवल पर्यावरण शुद्ध करता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। शंख भारतीय धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न अंग है। इसे पवित्रता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। शंखनाद से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है।
भारतीय संस्कृति के शुभ प्रतीक चिह्न हमारी धार्मिक आस्थाओं, जीवन मूल्यों और सामाजिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा हैं। ये चिह्न न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि हमें जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा भी देते हैं। इन प्रतीक चिह्नों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की गहराई और व्यापकता को समझा जा सकता है। इनका संरक्षण और सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस अमूल्य धरोहर से प्रेरणा ले सकें।
निम्नलिखित शब्दों के अर्थ जानने के लिए उन पर कर्सर ले जाएँ:
संस्कृति Culture , विविधता Diversity , गहराई Depth , आध्यात्मिकता Spirituality , प्रतीक चिह्न Symbol , महत्त्व Importance , परंपरा Tradition , धार्मिक आस्था Religious Belief , मार्गदर्शक Guide , धरोहर Heritage , प्राचीन Ancient , कल्याणकारी Beneficial , समृद्धि Prosperity , अनुष्ठान Ritual , सकारात्मक ऊर्जा Positive Energy , संतुलन Balance , पूजनीय Revered , ध्वनि Sound , ब्रह्मांड Universe , अस्तित्व Existence , एकाग्रता Concentration , आत्मिक शुद्धता Spiritual Purity , प्रज्वलन Ignition/Lighting , पवित्रता Purity , सौंदर्य Beauty , दिव्यता Divinity , करुणा Compassion , पोषण Nutrition , अडिग Steadfast , उन्नति Progress , पर्यावरण संतुलन Environmental Balance , सतत प्रवाह Continuous Flow , गति Movement , औषधीय Medicinal , नकारात्मक ऊर्जा Negative Energy , सुदृढ़ Strengthened , प्रेरणा Inspiration , व्यापकता Vastness , संरक्षण Conservation , अमूल्य Priceless ।
गुरुवार, 2 जनवरी 2025
महाकुंभ: गंगा तट पर संस्कृति संगम
 |
| १४४ वर्ष बाद आया महाकुंभ -२०२५ |
महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, यह एक सांस्कृतिक संगम भी है, जहाँ विभिन्न समुदाय, विचारधाराएं, और कला रूप एकत्रित होते हैं। गंगा, जो भारतीय संस्कृति की जीवनधारा मानी जाती है, महाकुंभ का केंद्र है। इसके तट पर आयोजित अनुष्ठान, संगम स्नान, और धार्मिक प्रवचन भारतीय समाज के आध्यात्मिक मूल्यों को सशक्त करते हैं। महाकुंभ में स्नान का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति माना गया है। गंगा तट पर संत-महात्माओं और भक्तों का जमावड़ा केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसार नहीं करता, बल्कि यह मानव चेतना को उच्चतर स्तर तक पहुँचाने का माध्यम भी है। ऋषि-मुनियों द्वारा दिए गए प्रवचन, ध्यान और योग शिविर, तथा वैदिक मंत्रोच्चारण से समूचा वातावरण दिव्यता से भर जाता है।
महाकुंभ भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। यहाँ देश के कोने-कोने से आए लोग अपनी परंपराओं, वेशभूषा, और लोक कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। कठपुतली नृत्य, लोकगीत, और पारंपरिक नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम इस आयोजन को और भी आकर्षक बनाते हैं। मेले में लगने वाली प्रदर्शनियां भारतीय हस्तशिल्प, संगीत, और साहित्य को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करती हैं। महाकुंभ केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि शैक्षिक महत्व का भी आयोजन है। यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं, जिनमें विद्वान भारतीय परंपराओं, धर्म और दर्शन पर अपने विचार साझा करते हैं। यह आयोजन न केवल प्राचीन ग्रंथों के महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि समकालीन सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
महाकुंभ के दौरान गंगा की स्वच्छता और संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जाती है। यह आयोजन पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने का माध्यम बन गया है। संगम पर इकट्ठा होने वाले लाखों लोग 'स्वच्छ भारत' और 'गंगा स्वच्छता अभियान' जैसे अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। महाकुंभ का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह आयोजन विदेशी पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। वे इस महोत्सव को भारतीय संस्कृति और जीवन शैली को समझने का एक सुनहरा अवसर मानते हैं। इसके महत्व के कारण ही यूनेस्को ने वर्ष 2017 में इसे "मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर" के रूप में मान्यता दी है।
आज के डिजिटल युग में महाकुंभ ने अपनी प्रस्तुति को और व्यापक बनाया है। जिवंत प्रसारण, आभाषीय यात्रा, और सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से यह आयोजन विश्व के हर कोने तक पहुँचता है। गूगल मैप, युट्यूब आदि आधुनिक तकनीको के उपयोग ने इसे अधिक सुलभ और आकर्षक बना दिया है। महाकुंभ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा, और विविधता का जीवंत प्रतीक है। यह गंगा तट पर एक ऐसा संगम प्रस्तुत करता है, जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक संसार एक-दूसरे से जुड़ते हैं। प्राचीन ज्ञान, सांस्कृतिक विविधता, और सामाजिक समरसता का यह महोत्सव भारतीय सभ्यता की महानता को उजागर करता है। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो जीवन की शाश्वतता और पवित्रता को रेखांकित करता है।
इस प्रकार महाकुंभ भारतीय संस्कृति की उस धरोहर को जीवित रखता है, जो 'वसुधैव कुटुंबकम्' के सिद्धांत पर आधारित है और समस्त मानव जाति के कल्याण का संदेश देती है।
नई शब्दावली
शनिवार, 28 दिसंबर 2024
हमारी जीवन शैली (Lifestyle)
जीवन शैली (Lifestyle) का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह का वह तरीका जिससे वे अपने जीवन को जीते हैं। इसमें उनके दैनिक कार्य, आदतें, रुचियां, विचारधारा, सामाजिक व्यवहार, खान-पान, पहनावा, और जीवन के प्रति दृष्टिकोण शामिल होता है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उनकी संस्कृति, परिवेश, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्तर, और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं।
जीवन शैली के प्रमुख घटक:
- स्वास्थ्य और खानपान: खानपान की आदतें, व्यायाम, और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के तरीके।
- सामाजिक व्यवहार: दूसरों के साथ व्यवहार, सामाजिक जुड़ाव, और रिश्तों की गुणवत्ता।
- पेशेवर जीवन: कार्यक्षेत्र में सफलता और संतुलन बनाए रखने के प्रयास।
- आर्थिक स्थिति: धन की प्रबंधन शैली और उपभोग के तरीके।
- मनोरंजन और रुचियाँ: व्यक्ति का खाली समय सदुपयोग करना; जैसे कि संगीत सुनना, फिल्में देखना, खेल खेलना, या यात्रा करना।
- आध्यात्मिकता और विचारधारा: धर्म, दर्शन, और जीवन के प्रति दृष्टिकोण।
जीवन शैली का प्रभाव:
जीवन शैली न केवल व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालती है। एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने से व्यक्ति का जीवन अधिक सुखद और उत्पादक बन सकता है।
💐श्रद्धांजलि: आखिर क्यों रह गए श्रीनाथ, अनाथ?
जीवन और साहित्यिक योगदान
परिवार का विमुख होना: समाज का आईना
संस्कारों की चेतावनी और समाज का दायित्व
श्रद्धांजलि और प्रेरणाा
इस आलेख को सुनने के लिए इस ऑडियो बॉक्स को क्लिक करें -
बुधवार, 25 दिसंबर 2024
निर्देश / दिशा-निर्देश✍️लेखन (Writing instructions)
निर्देश / दिशा-निर्देश लेखन का मुख्य उद्देश्य किसी भी कार्य को व्यवस्थित और कुशलता से संपन्न करना है।
'निर्देश लेखन' और 'दिशा-निर्देश लेखन' के बीच मूल रूप से बहुत अधिक अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य किसी कार्य या प्रक्रिया के लिए स्पष्ट और व्यवस्थित जानकारी प्रदान करना है। फिर भी, दोनों के बीच कुछ बारीक भिन्नताएँ होती हैं।
1. निर्देश लेखन:
- केंद्र: निर्देश लेखन में सीधे और संक्षिप्त तरीके से किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों को समझाया जाता है।
- लक्ष्य: एक विशेष कार्य या प्रक्रिया पर केंद्रित।
- उदाहरण:
- परीक्षा कक्ष में पालन किए जाने वाले निर्देश।
- किसी उपकरण को चालू करने या उपयोग करने के तरीके।
- "कृपया पानी बचाने के लिए नल को बंद करें।"
2. दिशा-निर्देश लेखन:
- केंद्र: दिशा-निर्देश लेखन में व्यापक और विस्तृत तरीके से किसी प्रक्रिया, कार्य, या व्यवहार के लिए नियमों और अपेक्षाओं को प्रस्तुत किया जाता है।
- लक्ष्य: एक कार्य या प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उपयोगी जानकारी और सुझाव प्रदान करना।
- उदाहरण:
- किसी अभियान के लिए दिशा-निर्देश, जैसे स्वच्छता अभियान।
- यात्रा या आयोजन के लिए विस्तृत गाइडलाइन।
- स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के पालन के लिए दिशा-निर्देश।
मुख्य अंतर:
| पहलू | निर्देश लेखन | दिशा-निर्देश लेखन |
|---|---|---|
| स्वरूप | संक्षिप्त और सीधे। | विस्तृत और व्यापक। |
| लक्ष्य समूह | कार्य विशेष को पूरा करने वाले लोग। | प्रक्रिया या अभियान से जुड़े सभी व्यक्ति। |
| उदाहरण का स्वरूप | कदम-दर-कदम निर्देश। | नियम और सुझावों का संग्रह। |
संक्षेप में कहें तो, 'निर्देश लेखन' विशिष्ट और संक्षिप्त होता है, जबकि 'दिशा-निर्देश लेखन' अधिक विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। दोनों का उद्देश्य पाठक को मार्गदर्शन देना है, लेकिन उनका दायरा अलग-अलग होता है।
निर्देश लेखन की प्रमुख विशेषताएँ:
- स्पष्टता (Clarity): निर्देश स्पष्ट और संक्षिप्त होते हैं।
- सटीकता (Accuracy): सही और प्रासंगिक जानकारी दी जाती है।
- क्रमबद्धता (Sequence): सभी बिंदुओं को तर्कसंगत और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है।
- आज्ञा वाचक वाक्य (Imperative sentence): अधिकतर वाक्य आज्ञा वाचक रूप में होते हैं।
- सीधी भाषा: जटिल शब्दों से बचा जाता है और भाषा पाठक के स्तर के अनुसार होती है।
उपयोग:
- शैक्षणिक क्षेत्र में: परीक्षाओं या प्रकल्प के लिए निर्देश।
- घरेलू उपयोग में: उपकरणों के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश।
- सार्वजनिक क्षेत्र में: किसी कार्यक्रम, यात्रा या आयोजन के लिए निर्देश।
- सुरक्षा एवं स्वास्थ्य: आपातकालीन स्थितियों के लिए सुरक्षा निर्देश।
आदर्श उत्तर -
निर्देश लेखन
विद्यालय की परीक्षा के लिए निर्देश -
- समय का पालन करें: परीक्षा कक्ष में निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब होने पर परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- पहचान पत्र साथ रखें: सभी विद्यार्थियों को अपने विद्यालय का पहचान पत्र परीक्षा के समय साथ रखना आवश्यक है।
- परीक्षा सामग्री: परीक्षा के लिए केवल अनुमति प्राप्त सामग्री, जैसे पेन, पेंसिल, रबर, और ज्योमेट्री बॉक्स साथ लाएं। गैर-आवश्यक सामग्री लाने से बचें।
- मोबाइल फोन का निषेध: परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना सख्त वर्जित है।
- परीक्षा कक्ष में प्रवेश: परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले सभी विद्यार्थियों को चेकिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। अनुचित सामग्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- बैठने की व्यवस्था: अपनी सीट पर बैठने से पहले सीट नंबर और स्थान की पुष्टि करें। अन्यत्र बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- उत्तर पुस्तिका का उपयोग: उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने पर सबसे पहले अपना रोल नंबर, नाम (यदि निर्देशित हो), और अन्य विवरण सही-सही भरें।
- प्रश्न पत्र पढ़ने का समय: प्रश्न पत्र मिलने के बाद, पहले 10 मिनट केवल उसे ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इस दौरान उत्तर लिखने की अनुमति नहीं होगी।
- लिखावट और प्रस्तुति: उत्तर पुस्तिका में उत्तर साफ-सुथरे और सुगठित तरीके से लिखें। गंदे या अस्पष्ट उत्तरों के लिए अंक कट सकते हैं।
- अनुशासन बनाए रखें: परीक्षा के दौरान अनुशासन का पालन करें। किसी भी प्रकार की अशांति या बातचीत अनुचित मानी जाएगी।
- सहायता की अनुमति नहीं: परीक्षा के दौरान एक-दूसरे से बात करना, किसी से सहायता लेना, या उत्तरों की नकल करना सख्त वर्जित है।
- समय प्रबंधन: सभी प्रश्नों को हल करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करें। अंतिम समय में हड़बड़ी से बचें।
- उत्तर पुस्तिका का समर्पण: परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर पुस्तिका को ध्यानपूर्वक अपने पर्यवेक्षक को सौंपें। अपनी उत्तर पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं है।
- शिष्टाचार का पालन करें: परीक्षा समाप्त होने के बाद शांति बनाए रखें और अन्य विद्यार्थियों को परेशान न करें।
- विशेष परिस्थितियों में: यदि परीक्षा के दौरान कोई समस्या हो, जैसे प्रश्न पत्र में त्रुटि या अन्य कठिनाई, तो तुरंत पर्यवेक्षक को सूचित करें। बिना अनुमति कक्ष छोड़ने की कोशिश न करें।
आदर्श उत्तर -
दिशा-निर्देश लेखन
विदेश यात्रा हेतु दिशा-निर्देश :
- सभी छात्र निर्धारित समय पर विद्यालय के मुख्य गेट पर एकत्रित हों। देरी करने वाले छात्रों को यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अपने साथ विद्यालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र और पासपोर्ट अवश्य रखें। दस्तावेज़ों की एक अतिरिक्त फोटोकॉपी अपने बैग में रखें।
यात्रा के दौरान विद्यालय द्वारा दिए गए समूह और प्रभारी शिक्षक का पालन करें। किसी भी स्थिति में समूह से अलग न हों।
अपने बैग में केवल आवश्यक वस्तुएं रखें, जैसे कपड़े, दवाइयां, और यात्रा से संबंधित आवश्यक सामग्री। अतिरिक्त और अनावश्यक सामान लाने से बचें।
यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें। सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार शिष्ट और मर्यादित होना चाहिए।
विमान यात्रा के लिए सुरक्षा जांच के सभी नियमों का पालन करें। ज्वलनशील पदार्थ, तेजधार उपकरण, या अन्य प्रतिबंधित सामग्री साथ न लाएं।
समूह के प्रभारी द्वारा दी गई यात्रा कार्यक्रम का ध्यानपूर्वक पालन करें। प्रत्येक गतिविधि के समय और स्थान का पालन करें।
यात्रा के दौरान विद्यालय का ड्रेस कोड (यदि लागू हो) का पालन करें और अपने पहनावे को संस्कृति और मौसम के अनुसार रखें।
किसी भी समस्या या कठिनाई के मामले में तुरंत अपने समूह के प्रभारी शिक्षक को सूचित करें।
अपने पास थोड़ा नकद और डेबिट/क्रेडिट कार्ड रखें। पैसों का उपयोग सोच-समझकर करें।
विदेश में स्थानीय नियमों और कानूनों का सम्मान करें। किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल न हों।
भोजन और पानी का ध्यान रखें। केवल स्वच्छ और सुरक्षित भोजन का ही सेवन करें। अनजान स्रोतों से खाना खाने से बचें।
महत्वपूर्ण सामान, जैसे पासपोर्ट, वीजा, और मूल्यवान वस्तुएं अपने साथ सुरक्षित रखें। इन्हें दूसरों को न सौंपें।
यात्रा के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का कचरा सार्वजनिक स्थानों पर न डालें।
यात्रा समाप्त होने के बाद सभी छात्र निर्धारित समय पर वापस विद्यालय पहुंचें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।
इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने से यात्रा सुरक्षित, आनंदमय और सुव्यवस्थित रहेगी।
अभ्यास प्रश्न:
इन प्रश्नों के अभ्यास से आपको विभिन्न अवसरों पर दिशा-निर्देश लेखन का अभ्यास मिलेगा और वे बेहतर ढंग से इसे समझ पाएंगे।
प्रचलित पोस्ट
-
छात्रों को निम्नलिखित लेखन विधाओं का अभ्यास करना अपेक्षित है - क) लेखन विधाएँ पत्र लेखन : (अनौपचारिक, औपचारिक और कार्यालयीन (व्यावसायिक) प...
-
परिचय - पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसमें व्यक्ति अपने विचार, अभिव्यक्ति, अनुभव या जानकारी को लिखित रूप में दूसरों के साथ साझा करता है। यह एक प...
-
नोट लेखन किसे कहते हैं? जब आप किसी विषय विशेष पर कोई महत्त्वपूर्ण सूचना, जानकारी अथवा विचारों संक्षिप्त रूप में लिखते हैं ताकि आप उन्हें बाद...
-
ईमेल किसे कहते हैं? ईमेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसका उपयोग विशिष्ट एक्सेस कोड का प्रयोग करते हुए दूरस्थ स्थानों (distanced places) ...
-
"किसी घटना, कार्य-योजना, समारोह अथवा शोध आदि के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखकर या छानबीन करके तैयार की गई लिखित सामग्री...
विशिष्ट पोस्ट
झजरिया: संस्कृति की सुगंध और परंपरा की मिठास भरी कहानी
झजरिया: संस्कृति की सुगंध और परंपरा की मिठास भरी कहानी दादी सुनाती, झजरिया की कहानी गर्मियों की छुट्टिय...





%20on%20Indian%20society.%20The%20image%20should%20feature%20a%20futuristic%20India%20with%20AI-dri.webp)